
हिंदी के सबसे बड़े रचनाकार प्रेमचंद की आज जयंती है। कई लोग उन्हे गांव, किसान से जुड़ा कथाकार भर समझते रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद उन दिनों फिल्मों के लिए लिखने बंबई भी गए थे। ये अलग बात है वहां की दुनिया उन्हे ज्यादा रास नहीं आई और वो लौट आए। उनकी लिखी फिल्म ‘मिल मजदूर’ के बारे में हम पहले भी पोस्ट डाल चुके हैं। फिल्मी दुनिया से प्रेमचंद भले लौट आए लेकिन हिंदी साहित्य के साथ साथ बंबई की फिल्मों पर भी उनके साहित्य का लंबे अर्से तक असर देखा गया। प्रेमचंद और सिनेमा विषय पर ‘न्यू डेल्ही फिल्म फाउंडेशन’ द्वारा कुछ वर्ष पहले ‘पर्दे पर प्रेमचंद, सिनेमा की सद्गति’ नाम से एक लाइव ऑनलाइन परिचर्चा आयोजित की गई थी। इस सत्र का संचालन अमिताभ श्रीवास्तव जिसमें प्रेमचंद की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ और उस पर सत्यजित राय द्वारा 1977 में बनाई फिल्म पर जाने-माने शिक्षाविद्-समाजशास्त्री, लेखक और फिल्म स्कॉलर प्रोफेसर जवरीमल्ल पारख Jawari Mal Parakh ने एक दिलचस्प विश्लेषण प्रस्तुत किया था। पेश है उसी पर आधारित एक संक्षिप्त आलेख, जो मूल रूप से उन्ही के कथन का लिखित रूप है।
प्रेमचंद की कहानी ‘शतरंज के खिलाड़ी’ 1924 में प्रकाशित हुई थी। ये गदर से एक साल पहले यानी 1856 में जब लखनऊ को ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने अधिकार में ले लिया, तब से संबंधित कहानी है, यानी 70-75 साल बाद लिखी गई कहानी। ये ध्यान देने के बात है कि प्रेमचंद के सामने क्या मुद्दे थे।

प्रेमचंद आजादी की लड़ाई के दौरान के लेखक हैं और उनका पूरा लेखन, उनके उपन्यास, उनकी कहानियां एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित हैं और उसमें अपनी तरफ से हस्तक्षेप भी है। वो इतिहास को भी देखते हैं, वो ये जानना चाहते हैं अपने साहित्य के माध्यम से कि ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान गुलाम बन गया। उसमें उनके सामने लखनऊ एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि किस तरह से यहां के जो सामंत थे, उन्होंने बगैर लड़ाई किए अंग्रेजी सत्ता, कंपनी राज के सामने घुटने टेक दिए। ये पतन केवल सामंतों का नहीं था, ये जनता का भी पतन था। इस रूप में उन्होने ये कहानी लिखी, ये कहानी एक तरह से हिदुस्तान की आत्मालोचना थी कि हम गुलाम इसलिए बने क्योंकि हमने इस गुलामी से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया… बल्कि अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्यों सरेंडर किया, क्योंकि हमारे यहां परिस्थितियां इस तरह की हो गईं, हम विलासिता में डूब गए, हमारे अंदर अपने राज्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, उसके सम्मान की रक्षा के लिए जो त्याग होना चाहिए, जो संघर्ष होना चाहिए… वो सब नहीं था।
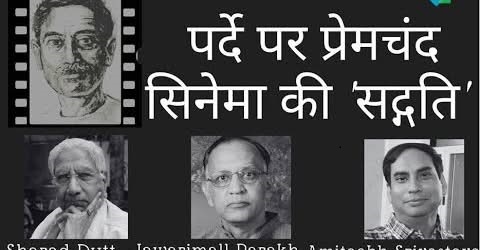
इस कहानी के शुरु में प्रेमचंद जो लखनऊ का वर्णन करते हैं, उस लखनऊ के वर्णन में वो जनता के पतन की कहानी बता रहे हैं, और जो सामंत वर्ग है उसके पतन की कहानी हमारे सामने आती है मीर और मिर्ज़ा के माध्यम से। तो एक तरह से वो कह रहे थे कि वो पूरा का पूरा समाज पतनशील समाज था और ऐसे पतनशील समाज का गुलाम बनना बहुत ही स्वाभाविक है।
लेकिन एक दूसरी चीज़ और है। प्रेमचंद की ये कहानी जहां से शुरू होती है और जहां समाप्त होती है वो दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु हैं। वो पहले बताते हैं कि क्यों हमारा देश गुलाम हुआ, लखनऊ की घटना, वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ के माध्यम से, मीर और मिर्ज़ा के माध्यम से ये बताते हैं। लेकिन जब अंत में वाजिद अली शाह को पकड़ कर कोलकाता ले जाया जा रहा है मटिया बुर्ज़ से, उस समय मीर और मिर्ज़ा एक छोटी सी बात पर तलवारें निकालते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि वो कायर नहीं थे, वो वीर थे, और उन्हे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। उससे बचने के लिए वो दूर खंडहरों में आकर शतरंज खेलते हैं, लेकिन वो बहादुर थे, इसलिए उन्होने अपने आप को मार लिया।

ये दो चीजों का संकेत हैं। एक तो संकेत इस बात का है कि हिंदुस्तान में जो सामंतवाद था, वो आत्मघाती सामंतवाद था। वो दूसरों से नहीं बल्कि खुद ही आपस में लड़-झगड़ कर मरने वाला सामंतवाद था। हमारा देश 1757 से लेकर 1857 तक लगभग सौ साल के दौरान धीरे-धीरे क्यों गुलाम होता गया, क्योंकि यहां के जो राजा-महाराजा थे, नवाब थे, वो अंग्रेजों से जब लड़ाई होती थी, तो दूसरे उसकी मदद के लिए नहीं आते थे। और इस तरह से धीरे-धीरे करके पूरा देश गुलाम बन गया। लेकिन जब मीर और मिर्ज़ा मर जाते हैं, तो वो भविष्य की ओर संकेत करते हैं। मीर और मिर्ज़ा का मरना दरअसल प्रेमचंद के लिए प्रतीकात्मक है प्रेमचंद के लिए कि वो सामंतवाद का मरना है, सामंतवाद मरणासन्न है, सामंतवाद का अंत होना है। ये जो आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये केवल साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं है, प्रेमचंद की दृष्टि में…. वो सामंतवाद के विरुद्ध भी है। ये सामंतवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है, इसका प्रतीकात्मक रूप वो दिखाते हैं मीर और मिर्ज़ा के आपस में एक दूसरे को मार डालने में। तो इस रूप में आप देखेंगे कि प्रेमचंद अपने समय में यानी की 1856 की घटना में वो सामंतवाद को भी इस रूप में देखते हैं और इस तरह से भविष्य में सामंतवाद की मृत्यु की घोषणा करते हैं।

