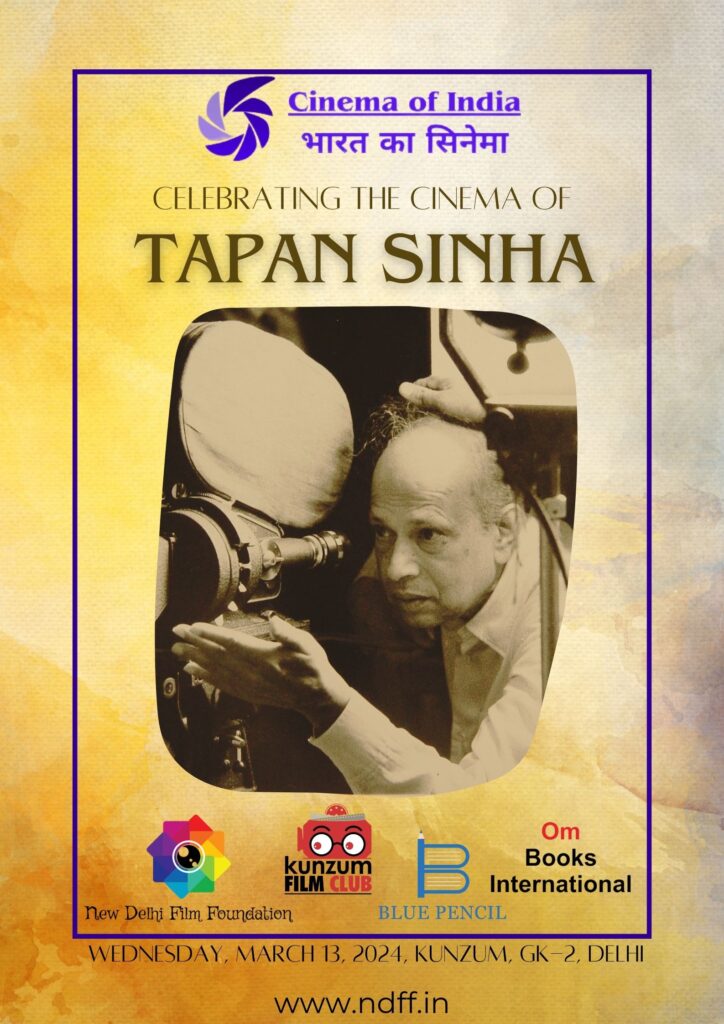अरुण खोपकर की ‘चलत् चित्रव्यूह’ अब हिंदी में


फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टिट्यूट, पुणे से सिने-दिग्दर्शन में स्वर्णपदक सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त अरुण खोपकर, प्रयोगशील सिने-दिग्दर्शक, प्रतिभाशाली विचारक और सिने-अध्येता इन तीनों रूपों में आधी सदी से भी अधिक समय से कार्यरत हैं। काव्य, स्थापत्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला विषयों पर शॉर्ट फ़िल्म्स और ‘कथा दोन गणपतरावाची’ तथा ‘हाथी का अंडा’ इन दो दीर्घ फ़िल्मों का दिग्दर्शन भी उन्होने किया है। पंद्रह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तथा देश के सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक तथा फ़िल्मों के लिए तीन बार स्वर्णकमल प्राप्त अरुण खोपकर की पुस्तक ‘गुरुदत्त : तीन अंकी शोकांतिका’ को सिनेमा से संबंधित सर्वोत्तम पुस्तक का राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में सिने-दिग्दर्शन पर शोधकार्य तथा अध्यापन में रत अरुण खोपकर की मराठी संस्मरण पुस्तक ‘चलत् चित्रव्यूह’ को साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला था। इसका हिंदी अनुवाद साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रस्तुत है इसकी विस्तृत समीक्षा अजय कुमार शर्मा द्वारा। पत्रकारिता और साहित्य सृजन में लंबा अनुभव रखने वाले अजय कुमार शर्मा चार दशकों से देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, संस्कृति, नाटक, इतिहास, सिनेमा और सामाजिक विषयों पर निरंतर लेखन करते रहे हैं। पिछले दो वर्षों से सिनेमा पर साप्ताहिक कॉलम “बॉलीवुड के अनकहे किस्से” का नियमित प्रकाशन हो रहा है। वर्तमान में वो दिल्ली के साहित्य संस्थान में संपादन कार्य से जुड़े हैं।

इस पुस्तक समीक्षा के साथ ही ‘न्यू डेल्ही फिल्म फाउंडेशन’ पर आप सिनेमा से जुड़ी नई पुस्तकों (पुरानी और महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी) की नियमित रुप से जानकारी पा सकेंगे और उनकी समीक्षा भी पढ़ सकेंगे। इसके अलावा हम उन पुस्तकों पर अपने यूट्यूब प्लैटफॉर्म पर भी चर्चा का आयोजन करेंगे। सिने बुक रिव्यू के नाम से शुरु इस पहल के लिए हम रचनाकारों, समीक्षकों और प्रकाशकों के सहयोग के आकांक्षी हैं। अधिक जानकारी के लिए ई मेल पर संपर्क करें ndff.india@gmail.com
‘चलत् चित्रव्यूह’ साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत मराठी संस्मरण की पुस्तक है जिसके लेखक हैं अरुण खोपकर। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है प्रकाश भातम्ब्रेकर ने। इसमें सिनेमा और कला जगत के विभिन्न पक्षों से जुड़े 11 महत्वपूर्ण लोगों के संस्मरण हैं। क्योंकि इसके लेखक अरुण खोपकर खुद फिल्मकार और अन्य कला माध्यमों से जुड़े रहे हैं इसलिए यह पुस्तक इतनी पठनीय और ज्ञानवर्धक है कि इससे हम जहां जिन व्यक्तियों पर संस्मरण लिखे गए है उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से रूबरू होते हैं वहीं उनके पूरे सृजन संसार और उस समय का परिवेश भी हमारे सामने आलोकित हो उठता है । यह संस्मरण बहुत ही आत्मीयता और और उनकी प्रतिभाओं के गहन अध्ययन और विवेचन के साथ लिखे गए हैं । इस तरह एक खास भावबोध के साथ लिखी गई पुस्तकों का अनुवाद बड़ा मुश्किल होता है और शायद ऐसे समय में प्रकाश भातम्ब्रेकर जी जैसे अनुभवी और वरिष्ठ अनुवादक की उपादेयता सिद्ध होती है। प्रकाश जी ने इसका ऐसा अनुवाद किया है कि पढ़ते हुए कहीं लगता ही नहीं कि हम कोई अनुवाद पढ़ रहे हैं। जिस भावुकता के साथ यह संस्मरण लिखे गए हैं लगभग उसी भावभूमि पर इनका अनुवाद भी किया गया है।अनुवाद का यही विशिष्ट रूप है जो उसे कई बार मूलकृति से भी अधिक सृजनात्मक और महत्वपूर्ण बना देता है ।

(अनुवादक का परिचय) प्रकाश भातम्ब्रेकर: हिंदी-मराठी-हिंदी अनुवादक। विगत लगभग पाँच दशकों से अनुवाद कार्य से संबद्ध। अब तक मराठी से हिंदी में अनूदित पुस्तकें 55 के आसपास इनमें उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संकलन, निबंध, पर्यावरण आदि । हिंदी से मराठी में भी छ: पुस्तकें अनूदित। कई दूरदर्शन कार्यक्रमों में सहभाग तथा संचालन। यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका समेत पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादेमी, भारतीय अनुवाद परिषद, नयी दिल्ली, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार समेत अन्य सरकारी तथा साहित्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ द्वारा सौहार्द सम्मान (2017)। एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई के अध्ययन मंडल के सदस्य के तौर पर दस वर्षों तक सहभाग।
पुस्तक का पहला संस्मरण ‘कलर्स ऑफ ऐबसेन्स’ है जिसमें वे प्रख्यात चित्रकार जहाँगीर सबावाला की मृत्यु पर फ़िल्म बनाने के अपने संस्मरण को तो साझा करते ही हैं बल्कि उसके सहारे उनके पूरे व्यक्तित्व की जाँच-परख भी करते हैं। वे बताते हैं कि सबावाला की कलायात्रा को अधोरेखित करने वाली फ़िल्म बनाने के दौरान 1993 में पहली बार हमारी व्यावसायिक मुलाक़ात हुई थी। यह फ़िल्म बनाने में एक साल से भी कुछ अधिक समय लगा। इस दौरान उनके घर में, स्टूडियो में घंटों हमारी बातचीत हुई थी, बहसें होती रहीं थीं। एक उम्दा कलाकार और संजीदा व्यक्ति के रूप में समझने-जज़्ब करने में हमारी ये मुलाक़ातें काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हुईं। जहाँगीर ने क्लासिक अकादमिक, इंप्रेशनिस्ट तथा क्यूबिस्ट शैली में शिक्षा प्राप्त की थी। इन शैलियों के मर्मस्थानों की पूरी जानकारी उन्हें थी। तथा उन्हीं का सुचारु प्रयोग कर सौंदर्य की थाह पाने का सफल प्रयास उन्होंने किया। अपनी स्वतंत्र व्यक्तिक पहचान बनाने की दिशा में वे बहुत देर से अग्रसर हुए। संस्मरण के अंतिम शब्दों को देखिए… सबावाला ने भले ही आँखें मूंद ली हों, किंतु उनकी चित्रमय आँखें बराबर खुली हैं तथा उनमें छुपा सौंदर्य आप ही हमारे सामने उजागर हो जाता है।

“संत भूपेन” में वे एक और कलाकार भूपेन खक्कर को याद करते हैं। बात उनकी स्मृति में हो रही शोक सभा से शुरू होती है और फिर उनकी चित्रकला, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, उनके सनकीपन, उनके ऊबड़-खाबड़ स्वभाव, उनके बचपने और खुद्दार कलाकार, उनमें समाया असाधारण बेजोड़ एवं शिखर पुरुष का महत्त्वाकांक्षी व्यक्तित्व, जो कभी नितांत अकेला तो कभी दोस्तों का कायल, तुनक मिज़ाज यानि भूपेन ‘टच’ की पर्त-दर- पर्त उभरने लगती है। इस पर्त में कई किस्से छिपे हैं जो अरुण जी साझा करते चलते हैं। उन्होंने चित्र बनाते समय भूपेन के सुध-बुध खो बैठने, उनके मुटल्ले किंतु संतुलित शरीर , उनके गायन, नाटकों और नाटकीयता में उनकी रुचि, कैमरे के आगे उनकी सहजता, कैनवास पर धीरे-धीरे रंग भरने की चर्चा भी की है। उनके चित्रों की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि मोची, नाई, घडीसाज, आदि उनकी तरह ही “कारीगर” थे और भारतीय चित्रकला को नया आयाम प्रदान करने वाले हैं। अंत में वे लिखते हैं कि उनके काम में शांत-सच्चा आत्मविश्वास और बेवाक निस्सिमता थी। धूल-गुबार अथवा ढोल-नगाड़े अथवा इश्तिहारबाजी के बिना आगे बढ़ते रहने के कायल थे वे।

अगला संस्मरण ग्राफिक्स आर्टिस्ट, फॉन्ट डिज़ायनर , कवि, विज्ञापन कंपनी ‘उल्का’ के निदेशक और मुंबई हैप्पीनिंग के प्रेणता रघुनाथ कृष्णराव जोशी पर है जिन्हें वह संक्षिप्त में र. कृ. से संबोधित करते हैं। वे पहले पहल उनसे तब मिलते हैं जब वे एफ. टी. आई, आई. पुणे के छात्र थे और अपनी पहली शॉर्ट फिल्म ‘तीव्र माध्यम ‘ के लिए टाइटल्स बनवाने थे। फांट यानि शब्दों को लिखने की कला जिसे सुलेखन, टाइपोग्राफी या छपाई कला भी कहा जाता है, विज्ञापनों की साज-सज्जा से लेकर ग्रीटिंग कार्ड, पुस्तकों की डिज़ायन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स को दर्शनीय और पठनीय बनाती है। इस कला की चर्चा बहुत इसलिए नहीं हो पाती है कि सामान्यतः कम लोगों का वास्ता इससे पड़ता है। अरुण उन्हें सबसे पहला महाराष्ट्रीय सुलेख कलाकार मानते हैं और बांग्ला में सत्यजित रे, पूर्णेदु पत्नी को। वे र. कृ. को विश्वस्तरीय कलाकार का दर्जा देते हैं।
दादू इंदुरीकर एक लोक कलाकार थे। उनकी विदूषक, मुखौटा कलाकार और हरफनमौला मसखरे की छवि को प्रस्तुत करते अपने संस्मरण में अरुण खोपकर बताते है कि कैसे एक लोक कलाकार बिना सुख-सुविधाएँ पाए अपनी कला को सुधारतेऔर निखारते हैं। हनुमान थिएटर (लालाबाग परिसर) में तमाशा कलाकारों के साथ अस्त-व्यस्त रहते इस कलाकार से वे कई बार वहीं मिले और उनसे बातचीत कर उन्हें जानने-समझने की कोशिश की। बातचीत से ज्ञात होता है कि इस प्रशिक्षण की शुरूआत बचपन से ही बदन को लचीला बनाने की प्रक्रिया से होती है। इसी दौरान संगीत, गायन, ढोलकवादन, नृत्य आदि की शिक्षा भी चलती रहती है। मुखौटा कलाकार अनपढ़ भले हों पर अशिक्षित नहीं होते बल्कि कई मायनों में सुशिक्षितों से बीस ही होते हैं।
अगला संस्मरण मराठी कविता का नया मुहावरा गढ़ने और उसे नई जुबान और सधे हुए कान देने वाले कवि नारायण गंगाराम सुर्वे पर है। उनकी कविता सुनाने की विशेषता का खाका खींचते हुए वे लिखते है,” नारायण सुर्वे की कविता सुनना एक इवेंट से कम नहीं होता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे कविता पढ़ रहे हैं। बल्कि वे श्रोताओं से सहज संवाद साध रहे होते थे। उनके काव्य वाचन में नाट्य होता था, निवेदन होता था पर अहंकार नहीं। उनके काव्य-पाठ में आरोह-अवरोह बाक़ायदा महसूस किए जा सकते थे, जिसमें नाराज़गी, करुणा, शोखी,वे एक सुरीले, ता रोमांच आदि सभी भाव मौजूद रहते थे। आगे वह कहते हैं कि उनके लोक तथा काव्य पाठ में नाट्य अवश्य है किंतु नाटकीयता नहीं। सुर्वे के अधिकांश पात्र समाज के दबे-कुचले कुनबे के होते हैं। कामगार वर्ग से उनकी निकटता महज़ अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं थी बल्कि उनकी जीवन शैली से संबद्ध थी । अगला संस्मरण “खंड क्रमांक शून्य “शीर्षक से प्रख्यात स्थापत्य शास्त्री (आर्किटेक्ट ) चार्ल्स कोरिया पर है जिनसे खोपकर जी का परिचय स्थापत्य कला पर एक फिल्म की कल्पना के समय होता है। मुंबई में बचपन बिता रहे चार्ल्स के पिताजी का निधन उनके लड़कपन में ही हो गया था और वे अपनी दादी के साथ बलार्ड पियर इलाके में रहते थे और हर शनिवार डॉक्स की सैर करते थे। वहीं जहाजों के भव्य काफिलों को देखकर उनकी परिकल्पनाओं ने उड़ान भरी। खिलौना ट्रेनों की वजह से भी वे स्थापत्यकला की ओर आकर्षित हुए।1958 में स्थापत्य शास्त्र में अमरीकी उच्चशिक्षा पूरी कर भारत लौटने के बाद साबरमती किनारे गाँधी स्मृति संग्रहालय के निर्माण का चुनौती पूर्ण कार्य उनके जिम्मे आ गया। दिल्ली में नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम को भी चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। मुंबई के पेडर रोड पर ‘कंचनजंघा ‘ इमारत, जयपुर का जवाहर कला केंद्र, सिदाद द गोवा, गोवा कला अकादमी, दिल्ली की ब्रिटिश काउंसिल, भोपाल की विधानसभा, गुजरात का अदालजी कुआँ, लिस्बन का शांपलिमों सेंटर फॉर दि अननोन’ आदि कुछ यादगार इमारतों के डिजायन गोवा निवासी चार्ल्स कोरिया के ही हैं।

‘पहला पर्दा, सफेद चॉक और ब्लैक बोर्ड’ शीर्षक वाले संस्मरण में वे एफ. टी.आई. आई. पुणे के अपने प्रोफेसर सतीश बहादुर को याद करते हैं। खोपकर उनके पढ़ाने के ढंग का विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहादुर साहब को सिनेमा के अलावा संगीत, साहित्य, चित्रकला आदि में भी गहरी रूचि थी। वे छात्रों को जब तक समझाते थे जब तक वे पूरी तरह से न समझ जाए और ऐसा करते हुए वे बिलकुल थकते नहीं थे। अध्यायक में विद्वत्ता के अलावा स्नेह, दयालुता, अनुराग भी होना चाहिए जो उनमें था। वे उनके द्वारा फिल्म को कई बार दिखाने और हर बार उनके अलग अलग पक्ष जैसे कैमरा, ध्वनि, संगीत, संवाद आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करने को कहते जिससे फ़िल्म केवल कहानी न रहकर अनेक कलाओं का समुच्चय बनकर सामने आती । चॉक और ब्लैक बोर्ड के बिना उनका काम नहीं चलता था। अंत में वे लिखते है कि ज़रूरी नहीं कि महान कलाकार उतना ही महान अध्यापक भी हो और महान अध्यापक उतना ही उम्दा कलाकार हो। बहादुर साहब ने खुद फिल्में तो नहीं बनाई , किंतु वे एक महान गुरु थे और समर्पित अध्यापक थे।
अगले संस्मरण में उन्होंने संगीतकार भास्कर चंदावरकर को याद किया है। भास्कर चंदावरकर ने काफी समय एफ.टी.आई पुणे में संगीत भी पढ़ाया था। भास्कर की बहुमुखी प्रतिभा को याद करते हुए वे “घासीराम कोतवाल” नाटक के लिए दिए गए उनके संगीत को भारतीय संस्कृति के अनुरूप मानते हुए बीसवीं सदी के रंगमंच के लिए अमूल्य धरोहर मानते हैं। भास्कर एफ.टी.आई में उस समय संगीत विभाग में थे जब ऋत्विक घटक वहाँ अध्यापक थे। वहाँ के मशहूर ‘विजडम ट्री’ के नीचे उनकी संगीत क्लास लगती थी। अंत में फ़िल्मों में उनके दिए संगीत की चर्चा है। फिल्म इंस्टीटयूट के कई छात्र शिक्षा पूरी कर लेने के बाद भी उनसे जुड़े रहे। माया दर्पण, माया मिरिगाा, अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? जैसी कई लो बजट फिल्मों और लीक से हटकर फिल्म बनाने वाले निर्देशकों की आर्थिक मुश्किलों के चलते भास्कर को भारतीय न्यू वेव सिनेमा का आधार स्तंभ कहा जा सकता है।

कैमरामैन के. के. महाजन पर है उनका अगला संस्मरण जो उनके द्वारा अभिनित पहली फिल्म “आषाण का एक दिन” के कैमरामैन थे और बाद में उनके गहरे मित्र बने और उनके द्वारा निर्देशित कई शॉर्ट फिल्मों के कैमरामैन भी । इससे पहले उन्होंने मणि कौल की श्वेत-श्याम फिल्म “उसकी रोटी ” अमृता शेरगिल की शैली में की थी यानि भारतीय चेहरों की मायूसी, मुफलिसी और बेबसी का चित्रीकरण । अरुण खोपकर उनकी प्रकाश व्यवस्था के भी बेहद कायल थे और उनकी मुस्तैदी के भी जिस कारण कई कम बजट के फिल्मकार फिल्म बनाने की हिम्मत कर पाते थे। 70 के दशक में फिल्मों की अलग दुनिया ‘सारा आकाश’ (बासु चटर्जी) ‘उसकी रोटी’ (मणि कौल ) ‘भुवन शोम’ (मृणाल सेन) को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ उकेरा था। नई पीढ़ी उनसे क्या सीखे के जवाब में खोपकर कहते हैं कि उन्हें देश की बदलती ऋतुओं, फल-फूल, पेड़- पौधों, गोरे-काले चेहरों की विविधता को वास्तविक लोकेशन्स पर पकड़ने का हुनर सीखना चाहिए।
मणि (मनी) कौल को उन्होंने ‘जो न देखे रवि ‘ शीर्षक से लिखे अपने संस्मरण में याद किया है। यादों का सिलसिला 6 जुलाई 2011 की अल-सुबह मनी की मृत्यु के संदेश से होता है जब मुंबई में धुंआधार बारिश हो रही थी। उन्हें मनी से अपनी अंतिम मुलाकात जो दिल्ली में फरवरी में हुई थी कि याद आ जाती है जब वे उनके गले मिले थे और बीमारी के कारण इतने जर्जर हो चुके थे कि उनकी पसलियाँ उन्हें चुभ रही थीं। आगे वे उन्हें याद करते हुए लिखते है कि वे थे तो कश्मीरी लेकिन उनका बचपन जयपुर में बीता। प्रख्यात फिल्म-निर्देशक महेश कौल उनके चाचा थे। उनका असली नाम रवींदनाथ था । शुरूआत की फिल्मों में उन्होंने अपना नाम लिखा मनी कौल और बाद में मणि कौल लिखा। मनी की शार्ट फिल्मों की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि मनी ने अपनी सृजनात्मकता से इस विद्या को चार चाँद लगा दिए। बाद में वे उनकी दो अन्य फीचर फिल्मों ‘दुविधा’ और ‘नौकर की कमीज़’ का उल्लेख करते हुए उन्हें युवा प्रेमीजनों की अंतरंगता के क्षणों को कैद करने वाली उच्च कोटि की नाट्य निर्मिती मानते हैं।
पुस्तक का अंतिम संस्मरण “रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल” में वे ऋत्विक घटक के सृजनात्मक संसार को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ऋत्विक घटक की प्रतिभा का अंतिम उद्रेक थी फिल्म ‘जुक्ति, टाक्को आर गापो’ (1974) । इसमें वे ख़ुद ही नायक नीलकंठ बने थे। यह फिल्म माने ऋत्विकदा का हूबहू प्रतिबिंब है। खंडित व्यक्तित्ववाला, विस्थापित, अनिकेत बना एक बुद्धिमंत, होनहार नायक/कलाकार बंगाल के जंगलों, विभिन्न इलाकों की खाक छानता है, कई लोगों से मिलता है, विविध अनुभव प्राप्त करता है।
खोपकर ऋत्विकदा के कलाविकास की पहली सीढ़ी रंगमंच को मानते हुए “इप्टा” के लिए उनके नाट्य लेखन, अभिनय आदि का उल्लेख करते हुए कहते है कि उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली ऐतिहासिक घटना थी देश का विभाजन। विभाजन की त्रासदी ही ऋत्विकदा के सृजन की मूल प्रेरणा रही। इसी के चलते ‘मेघे ढाका तारा’ (1960), ‘कोमल गांधार’ (1961) तथा ‘सुवर्णरेखा’ (निर्मिति 1962, वितरण 1965) ये तीन फ़िल्में उन्होंने बनाईं। वे हमेशा ख़ुद को शरणार्थी ही कहते थे। वे पूछा करते थे, ‘कौन शरणार्थी नहीं है? बताओ?’
पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद लेखक अरुण खोपकर जी के भूमिका में लिखे इन शब्दों से शब्दशः सहमत हुआ जा सकता है कि,”एक चित्र जब दूसरे के साथ हमें जोड़ता है तभी तो वह अपने बेजोड़ होने की मिसाल बन जाता है। यही तो एक चित्र का दूसरे चित्र के ज़ेहन में परकाया प्रवेश है…”।