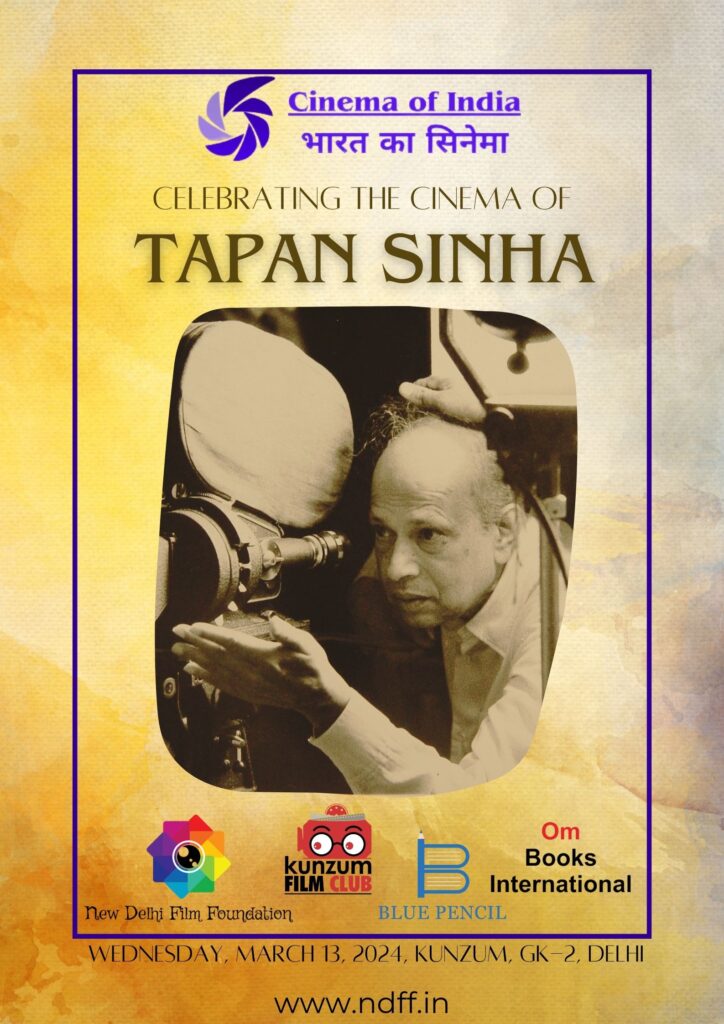सच्चे ‘जन कलाकार’ थे बलराज साहनी


हिंदी सिनेमा में जिन तीन अभिनेताओं का नाम स्वाभाविक अभिनय के चलते अदाकारी की दुनिया में बेहद ऊंचे मुकाम पर रखा जाता है, वो हैं मोतीलाल, दिलीप कुमार और बलराज साहनी। बलराज साहनी की पुण्यतिथि 13अप्रैल पर उन्हे याद कर रहे हैं लेखक अजय कुमार शर्मा। बुलंदशहर में जन्मे और बरेली में शिक्षा प्राप्त किएअजय कुमार शर्माने भारतीय जनसंचार संस्थान,दिल्लीसेहिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और हिंदी की पहली वीडियो समाचार पत्रिका “कालचक्र ” में कार्य के बाद लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शोध संयोजन, पटकथा एवं निर्देशन सहयोग किया। चार दशकों से देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, संस्कृति, नाटक, इतिहास, सिनेमा और सामाजिक विषयों पर वो निरंतर लेखन करते रहे हैं।पिछले दो वर्षों से सिनेमा पर साप्ताहिक कॉलम “बॉलीवुड के अनकहे किस्से” का नियमित प्रकाशन हो रहा है। वर्तमान में वो दिल्ली के साहित्य संस्थान में संपादन कार्य से जुड़े हैं।
बलराज साहनी ने अपने जीवंत अभिनय से जो भी भूमिकाएँ की उन्हें यादगार बना दिया। ‘धरती के लाल’ का गरीब किसान, ‘दो बीघा जमीन’ का हाथ से रिक्शा खींचने वाला मजदूर, ‘हम लोग’ का मुखर बेरोजगार युवा, हलचल का उदार जेलर, ‘काबुलीवाला’ का पठान या फिर अपनी अंतिम फिल्म ‘गरम हवा’ का मुस्लिम व्यापारी जो विभाजन की त्रासदी झेल रहा है… इन किरदारों को जब याद करते हैं तो हमें बलराज साहनी नहीं बल्कि ये किरदार ही सामने खड़े दिखाई देते हैं। बतराज साहनी ने अपने को इन किरदारों में इस तरह डाला कि वह गायब हो गए और दर्शकों को उनके किरदार ही याद रहे आए। ‘दो बीघा जमीन’ की कलकत्ता में हुई शूटिंग के दौरान कई बार भीड़ ने उन्हें असली रिक्शाचालक समझकर ही व्यवहार किया। यह उनके स्वाभाविक हुलिए और बोल चाल की वजह से ही हुआ, जिसके लिए उन्होंने स्वयं से कड़ी मेहनत की थी। बंबई के जोगेश्वरी इलाके में उत्तरप्रदेश और बिहार के भैंस पालने वाले भैया लोगों की बस्ती में उन्होंने उन के खान-पान, पहनावे बोलचाल का गहराई से अध्ययन किया। सिर पर गमछा बांधने का विचार उन्हें यही से आया था।
बलराज साहनी का फिल्मों में आना पूर्व नियोजित नहीं था। वह काफी सोच-समझकर ही फिल्मों से जुड़े थे और इस का कारण बने चेतन आनंद जो गवमेंट कालेज, लाहौर में उनके साथ पढ़े थे और उनसे दो साल जूनियर थे।

बलराज ने 1934 में अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ दिन रावलपिंडी में अपने पिता का कपड़ों का व्यापार संभाला। उनका मन इसमें लग नहीं रहा था। इस बीच 6 दिसंबर 1936 को उनकी शादी दमयंती (बलराज के मित्र जसवंत राय की छोटी बहन) से हुई। कुछ दिनों बाद ही उन्हें साथ ले लाहौर आ गए और यह यहाँ से ‘मंडे मार्निंग’ नामक एक साप्तहिक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला। दो-तीन अंक निकालते ही तबियत खराब होने के कारण इसे बंद कर दोनों पति-पत्नी कलकत्ता चले गए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ के पास, जो उनके सहपाठी के बड़े भाई थे। यहाँ कुछ दिन लेखन कार्य करने के बाद ‘अज्ञेय’ की सिफारिश पर उन्हें शांतिनिकेतन में हिंदी अध्यापक की नौकरी मिल गई। यहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। यह 1937 के जाड़ो की बात थी। लगभग दो साल यहाँ बिताने के बाद वे गाँधी जी के वर्धा स्थित सेवाग्राम जा पहुँचे ‘नई तालीम’ पत्रिका के सहायक संपादक बनकर यहाँ एक साल ही गुजरा था कि वे गाँधी जी की अनुमति लेकर बी.बी.सी. लंदन में उद्घोषक बनकर इंग्लैंड चले गए। वे यहाँ चार साल तक रहे। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था।
1944 की गर्मियों में साहनी दंपति इंग्लैंड से वापस लौटे। उनके साथ कुछ ही महीनों की उनकी बेटी शबनम थी। अपने बड़े बेटे परीक्षित को वे इंग्लैंड जाने से पहले दादा-दादी के पास रावलपिंडी छोड़ गए थे। इंग्लैंड से बलराज दंपति पूरी तरह बदलकर आए थे। अब वे एक पक्के मार्क्सवादी थे।
इंग्लैंड से वापसी में ये कुछ दिन बंबई में रुके। एक दिन बलराज की मुलाकात अचानक चेतन आनंद से हो गई जिन के साथ पढ़ते हुए लाहौर में उन्होंने कई नाटकों में साथ-साथ काम किया था ! चेवन से बातचीत के दौरान उन्हें जान कर खुशी हुई कि अब भारत में भी सभ्य समाज के लोग फिल्मों को उतनी बुरी नजर से नहीं देख रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन माध्यमों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। उन्हीं से उन्हें पता चला कि उपेन्द्र नाथ अश्क’, सआदत हसन मंटो, भगवती चरण वर्मा, जोश मलीहाबादी, अमृतलाल नागर, प. नरेंद्र शर्मा जैसे चोटी के लेखक बंबई में रहकर ही फिल्मों के लिए कहानियाँ और गीत लिखकर हजारों रुपए कमा रहे हैं।

इंग्लैंड जाने से पहले बलराज साहनी की भी गिनती हिंदी के युवा कहानीकारों में होने लगी थी। उनकी कहानियां “विशाल भारत’ ‘हंस’ और अन्य पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रही थीं। बबई में चेतन आनंद और उर्दू लेखक कृश्न चंदर (ये भी लाहौर में एफ. सी कॉलेज में पढ़े थे) से हुई मुलाकातों से बलराज ने इतना तो जरूर सोचा कि अगर कहीं और कुछ न हुआ तो दूसरे साथी लेखकों की तरह फिल्मों के लिए लिखकर तो रोजी-रोटी कमाई ही जा सकती है। अभिनय की बात अभी तक उनके दिमाग में नहीं आई थी।
इस बीच काफी समय के बाद उन्होंने एक कहानी लिखकर ‘हंस’ पत्रिका को भेजी। लेकिन वह अस्वीकृत हो गयी। बलराज के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। तभी चेतन आनंद ने उन्हें और उनकी पत्नी दमयंती को फिल्म ‘नीचा नगर में जिसका वह निर्देशन कर रहे थे के मुख्य पात्रों का रोल करने का प्रस्ताव रखा। अस्वीकृत कहानी से चोट खाए बलराज ने चेतन का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। इस तरह एक अस्वीकृत कहानी ने बलराज का फिल्मों में अभिनय करने का रास्ता खोल दिया।
सितम्बर 1944 में बलराज, दमयंती और दोनों बच्चों के साथ बंबई, चेतन आनंद के घर जा पहुँचे। आर्थिक मुश्किलों के चलते ‘नीचा नगर’ फिल्म की शूटिंग आरंभ नहीं हो पायी. चेतन और बलराज एवं दमयंती भी दूसरी फिल्मों में काम ढूंढने लगे। तभी उनका परिचय भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) में ख्वाजा अहमद अब्बास व अन्य प्रगतिशील नाट्य प्रेमियों से हुआ और ये पत्नी सहित शीघ्र ही इसका अहम हिस्सा बन गए और ताउम्र बने रहे। इस समय ‘इप्टा’ में देश की एक से एक प्रतिभाशाली हस्तियाँ काम कर रहीं थीं। सांस्कृतिक चेतना से भारतीय समाज को बदलने का यह अपने समय का सबसे बड़ा सामूहिक प्रयास था।
बलराज और उनकी पत्नी को कुछ फिल्मों जैसे ‘इंसाफ’ ‘दूर चलें’ ‘गुड़िया’ ‘हलचल’ में छोटे-मोटे रोल मिले। ‘इप्टा’ द्वारा बनाई गई एक मात्र फिल्म ‘धरती के लाल’ में दोनों ने मुख्य पात्रों की भूमिकाएं निभाईं। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दमयंती को पेट की बीमारीयों ने ऐसा घेरा कि 29 अप्रैल 1947 को वे अचानक चल बसी इस समय उनकी आयु मात्र 28 वर्ष थी और कुछ दिन पहले ही पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें पृथ्वी थियेटर की मुख्य अभिनेत्री का कान्ट्रेक्ट दिया था। जिंदगी ढर्रे पर लौट ही रही थी कि इस घटना ने बलराज को हिला कर रख दिया। इस बीच भारत विभाजन और साम्प्रदायिक दंगो ने उन्हें भावनात्मक रूप से गहरी चोट पहुंचाई। वे अपने दोनों बच्चों के साथ वापस श्रीनगर चले गए। इस हताशा की स्थिति में प्रसिद्ध लेखक अमृत लाल नागर आगे आए और उन्होंने अपनी लिखी फिल्म ‘गुंजन’ में मुख्य पात्र का रोल दिलवाया। उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत! अपनी खराब मनोस्थिति के चलते बलराज फिल्म में सहज अभिनय नहीं कर पाये और फिल्म फ्लॉप हो गयी।

मार्च 1949 में उन्होंने संतोष से दूसरा विवाह किया। संतोष उनकी फुफेरी बहन थी यह उनका भी दूसरा विवाह था। उनका पहला विवाह प्रसिद्ध लेखक ‘अज्ञेय’ से हुआ। दरअसल यह लड़कपन का प्यार था जिसके बारे में बलराज ने दमयंती से विवाह करते हुए उनके भाई जसवंत राय को भी बताया था। उस समय इसे कच्ची उम्र का ‘जुनून’ कहकर टाल दिया गया था। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के एक जुलूस में भाग लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वे छह माह जेल में रहे। इस बीच ‘हलचल ‘ फिल्म की शूटिंग के समय जिसमें से एक जेलर की भूमिका निभा रहे थे, के लिए समय-समय पर पैरोल पर लाए गए। मुश्किलों के इस दौर में उन्होंने चेतन आनंद के बैनर फिल्म के लिए ‘बाजी’ फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित यह पहली फिल्म थी। देव आनंद इसके हीरो थे। इस बीच जिया सरहदी की फिल्म ‘हम लोग’ जिसमें उन्होंने एक बेरोज़गार युवा का रोल किया था हिट रही। उनके अभिनय को जनता ने पसंद किया यह 1951 की बात है। इसके बाद उन्हें बिमल राय की फिल्म ‘दो बीघा जमीन’ में किसान शंभू महतो का रोल मिला। इस पात्र को जीवंत बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और इसका परिणाम भी चौंकाने वाला रहा। 1953 में प्रदर्शित हुई इस फिल्म से उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। देश ही नहीं विदेशों के भी कई बड़े पुरस्कार इस फिल्म को मिले।
इस फिल्म के साथ ही बलराज का संघर्ष खत्म हुआ। आने वाले 19 वर्षो में उन्होंने 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जबकि संघर्ष के पिछले दस सालों में उन्होंने मुश्किल से दस फिल्मों में भी काम नहीं किया था। दो बीघा जमीन के बाद आई उनकी कुछ महत्त्वपूर्ण फिल्में थी- सीमा’ (1954) गरमकोट (1955) कठपुतली’ (1997 ‘परदेशी’ (1987) ‘भाभी’ (1957) ‘लालबत्ती’ (1957) साने की चिड़िया’ (1957) लाजवंती’ (1958) हीरा-मोती (1959), ‘छोटी बहन’ (1959) ‘अनुराधा’ (1960) भाभी की चूड़ियाँ (1961) काबुलीवाला’ (1961) ‘अनपढ़’ (1962) ‘हकीकत’ (19) 64) (1965) पिंजरे का पंछी’ (1966) हमराज़ (1967) ‘संघर्ष’ (1968) ‘दो रास्ते’ (1969) ‘पवित्र पापी’ (1970) एवं गरम हवा’ (1975)।

“गरम हवा” उनकी अंतिम महत्त्वपूर्ण फिल्म थी, उनकी बेहतरीन अदाकारी का एक और यादगार नमूना . एम. एस. सथ्यू की यह फिल्म भारत-पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित थी। आगरा की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी के अनुसार उनके ज्यादातर रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए हैं और यह वहाँ जाएं न जाएं की स्थिति में घिरे हुए है। इस बीच उनकी बेटी हाथ की नस काटकर जान दे देती है। वह अपने लिए चुने गए दूल्हे के पाकिस्तान जाने और वहाँ शादी करने का समाचार सुन कर यह कदम उठाती है। बलराज ने अपनी संवेदना से इस दृश्य को अमर कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में विभाजन की त्रासदी तो देखी ही थी, कुछ दिन पहले (5 मार्च 1972) ही उनकी बेटी शबनम की भी असफल विवाह के चलते मृत्यु हुई थी। इस दृश्य में मानों उन्होंने अपनी वास्तविक जिंदगी का ही कोई हिस्सा खोया था।

फिल्म की डबिंग खत्म करते ही कुछ दिनों बाद 13 अप्रैल 1973 को उनकी मृत्यु हो गई थी। यह फिल्म 1974 में प्रदर्शित हुई। इसे वर्ष का राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिए जाने वाला राष्ट्रीय नर्गिस दत्त पुरस्कार दिया गया। कहानी और संवाद के लिए इस्मत चुगताई और कैफी आजमी भी पुरस्कृत हुए थे। इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कार के लिए इसे भारतीय प्रवष्टि के रूप में भेजा गया था और कांस फिल्म समारोह में इसे गोल्डन पाम पुरस्कार के लिए नामजद किया गया था।
आज बलराज साहनी हमारे बीच नहीं है, लेकिन लगभग साठ वर्ष के अपने जीवन में उन्होंने अपने को अधिक व्यापक क्षेत्रों में व्यक्त कर पाने के लिए कई कला-माध्यमों को चुना। उन्होंने केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अध्यापक, नाट्य लेखक-निर्देशक, रेडियो उद्घोषक, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ किया। उनके भीतरी और बाहरी रूप में कोई अलगाव न था। देश और देश की जनता के लिए कुछ बेहतर और अच्छा करने की बेचैनी ने उन्हें लाहौर, शांतिनिकेशन, सेवाग्राम(वर्धा), लंदन, बंबई और न जाने कहाँ-कहाँ घुमाया, लेकिन इन सभी जगहों से एक कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत कुछ पाया। उनकी सहज और स्वाभाविक अभिनेता की पहचान का कारण यह भी था कि वह अपने आसपास के सामाजिक परिवेश से कभी कटे नहीं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वह सफल और लोकप्रिय अभिनेता थे तब भी किसी दंगा-फसाद, प्राकृतिक प्रकोप, मजदूरों, फौजियों, युवाओं की सहायता के लिए प्रदर्शन आदि करने की जरूरत होती तो वह देश के किसी भी कोने में जाने को हमेशा तत्पर रहते! अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही वह महाराष्ट्र के सूखा ग्रस्त इलाकों का दौरा करके लौटे थे। भिवंडी में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय पहले तो वे भीष्म साहनी, ख़्वाजा अहमद अब्बास और आई. एस. जौहर के साथ गए थे और बाद में वहाँ अकेले ही दो हफ्ते मुस्लिमों की बस्ती में रहे थे।
देश की आम जनता से इस लगाव के चलते ही प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक ख्वाज़ा अहमद अब्बास ने उन्हें एक मात्र ‘जन कलाकार’ का खिताब दिया था जो उन पर हर लिहाज से फिट बैठता था। ‘मेरी फिल्मी आत्मकथा’ में उन्होंने स्वयं ही इस संबंध में लिखा है कि, “अभिनेता जनता के सामने जीवन पेश नहीं करता, दूसरों के जीवन की तस्वीर पेश करता है। ‘हमलोग’ फिल्म में मैंने एक पढ़े-लिखे बेरोजगार का पार्ट अदा किया, ‘दो बीघा जमीन’ में एक दुःखी किसान का, ‘औलाद’ में एक घरेलू नौकर का, ‘सीमा’ में एक विद्वान समाज सेवक का, ‘टकसाल’ में करोड़पति का और ‘काबुलीवाला’ में एक मुफलिस पठान का… सब रोल एक दूसरे से जुदा थे। अगर मैं किसानों, मजदूरों, पठानों वगैरह का जीवन करीब से जाकर न देखता तो यह कभी संभव नहीं हो सकता था कि मैं यह पार्ट अदा कर सकता। अगर उन्हें करीब से देखना उचित था तो उनके जीवन की आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को जानना और समझना भी मेरा फर्ज था, तभी में उनके दिलों की धड़कनों को अपनी आँखों और शब्दों में अभिव्यक्त कर सकता था, वरना बात अधूरी रह जाती…..।
ऐसे सच्चे जन कलाकार को नमन्।